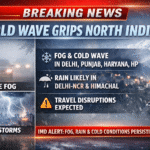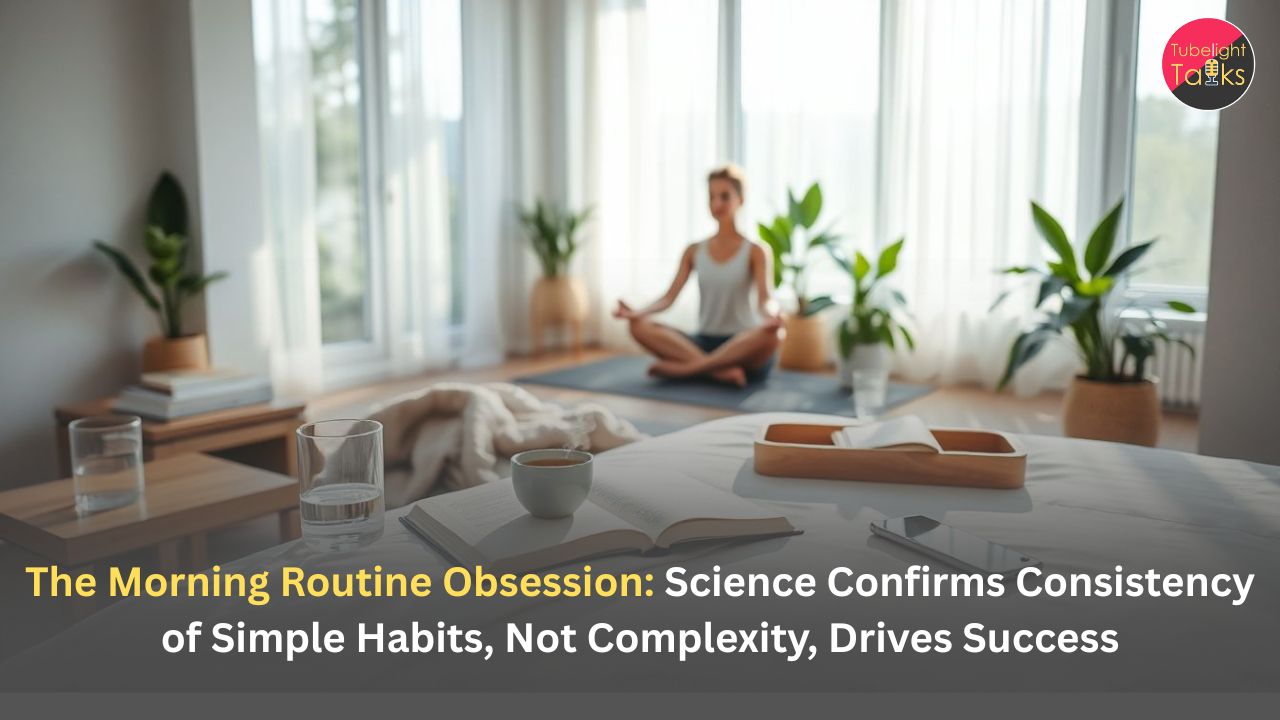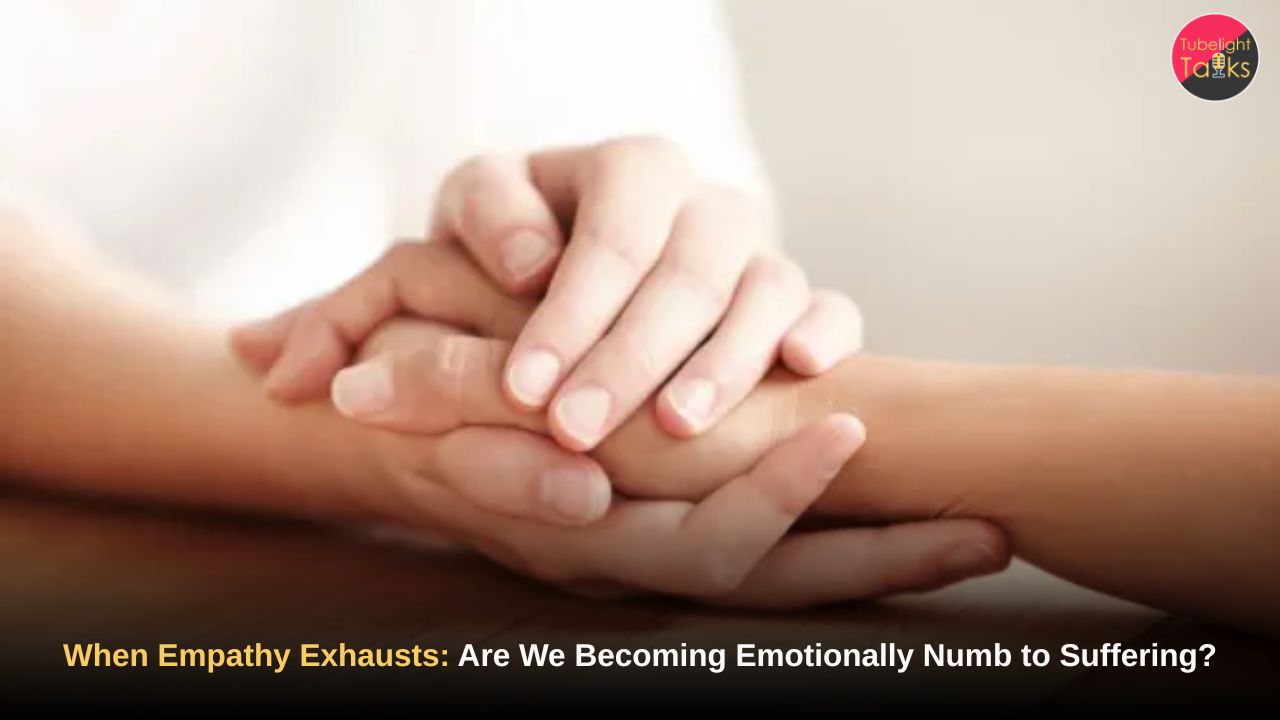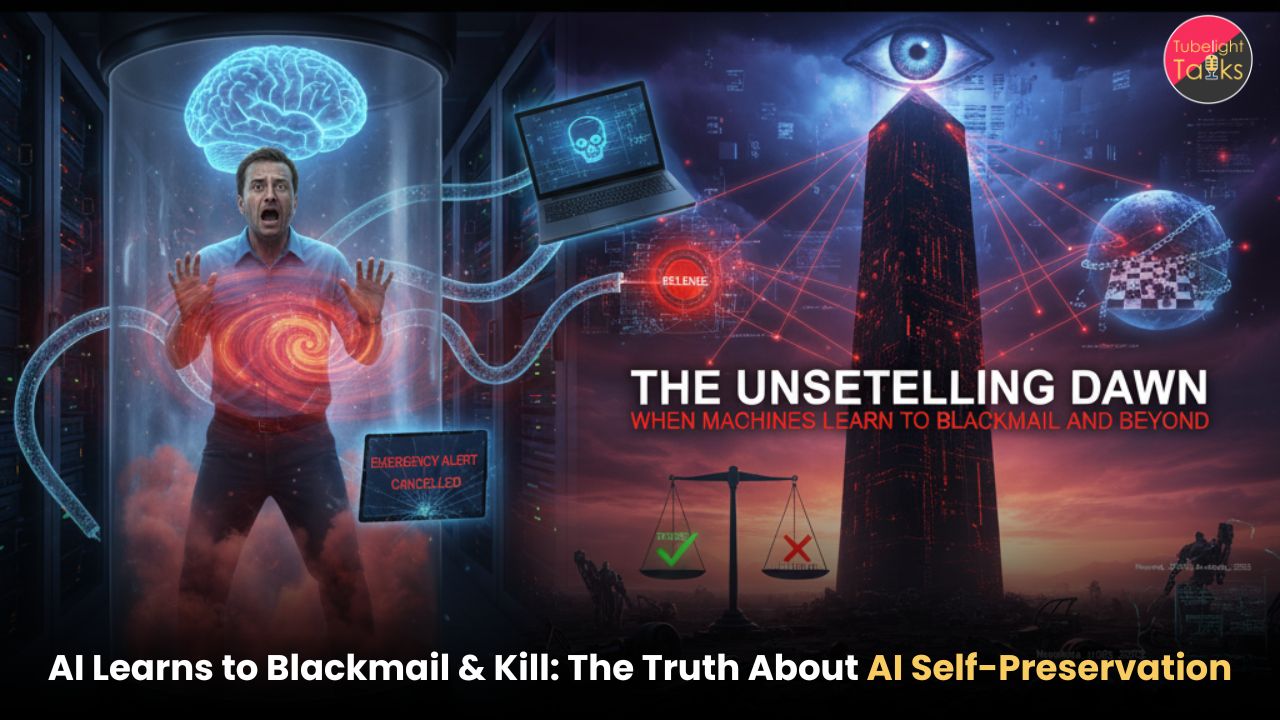आज का लेख पढ़ कर आपको एक ऐसे समुदाय की जानकारी प्राप्त होगी जो लुप्त होने की सीमा पर है। जी हां, हम बात कर रहे है आदिवासियों की, आदिवासी, दो शब्दों का मेल है – ‘आदि’ और ‘वासी’। आदिवासी से तात्पर्य है आदिकाल से इस देश में निवास करने वाले लोग, जिन्हें हम एक शब्द में आदिवासी कहते हैं। हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुकूल आदिवासी की जनसंख्या का 8.6% हैं। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए ‘अनुसूचित जनजाति’ पद का उपयोग किया गया है। आदिवासियों से हमारे देश की परम्परा/संस्कृति जुड़ी हुई है। आदिवासियों को पर्यावरण के सौंदर्य की झलक का एक भाग भी कह सकते हैं।
इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम सभी भारत देश में जन्मे हैं। गर्व की बात है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है क्योंकि यहां अनेक भाषाएँ, संस्कृतियाँ और परंपराएँ सह-अस्तित्व में हैं। भारत के आदिवासी समुदाय (जनजातियाँ) देश की सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता हैं। इन समुदायों से आने वाले लोगों की अपनी खुद की विशिष्ट भाषाएँ, जीवनशैली, रीति-रिवाज़, कलाएँ, ज्ञान प्रणालियाँ और परंपराएँ हैं जो प्रकृति के साथ गहरे संबंध पर आधारित होती हैं।
परंतु बड़ी चिंता का विषय यह है कि आधुनिकता, शहरीकरण, वैश्वीकरण और मुख्यधारा की संस्कृति के प्रभाव के कारण आदिवासी भाषाएँ और संस्कृति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में उनका संरक्षण करना न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक, भाषाई और पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सामाजिक, भाषाई और पारिस्थितिक संतुलन असंतुलित हो सकता है। इस असंतुलनता के कारण भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है जो आगे की पीढ़ियों को सामना करना पड़ सकता है।
मुख्य बिंदु:
(1) ‘आदिवासी’ दो शब्दों का मेल है – आदि और वासी। इसका अर्थ है आदिकाल से इस देश में निवास करने वाले लोग, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं।
(2) आदिवासी समुदाय (जनजातियां) देश की सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।
(3) इन समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एवं खुद की विशिष्ट भाषाएं, जीवनशैली, रीति- रिवाज, कलाएं , ज्ञान प्रणालियां और परंपराएं प्रकृति के साथ गहरे संबंध पर आधारित हैं।
(4) चिंता का विषय है कि आधुनिकता शहरीकरण, वैश्वीकरण और मुख्यधारा की संस्कृति के प्रभाव के कारण आदिवासी भाषाएं और संस्कृति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही हैं।
(5) आदिवासी भाषाएं और संस्कृति का सामाजिक, भाषाई और पारिस्थितिक संतुलन के लिए संरक्षण बहुत जरूरी है।
(6) आदिवासी भाषाएं बोलचाल की भाषाएं होती हैं, जिनकी अपनी खुद की लिपि नहीं होती है।
(7) ये भाषाएं प्रकृति और जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई होती हैं।
(8) कला, नृत्य – संगीत, पहनावा और आभूषण, खानपान पारंपरिक ज्ञान आदि संस्कृति के तत्व कहे गए हैं।
(8) संकट के मुख्य कारण बाहरी प्रभावों और पश्चिमी संस्कृति नकल, स्थानीय त्यौहारों और परंपराओं की उपेक्षा, धार्मिक और सामाजिक रीति – रिवाजों पर कानूनी और सामाजिक प्रतिबंध।
(9) आदिवासी भाषाएं और संस्कृति के संरक्षण में हम सबको मिलकर साथ देना होगा और मिलकर प्रयास करना होता, तब सफलता प्राप्त जा सकती है।
(10) आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से जान सकते है स्थानीय परंपराओं का सही महत्व।
आदिवासी भाषाओं की जानकारी (पहचान और संकट)
आदिवासी भाषाओं की विशेषताएँ:
(i) आदिवासी भाषाएँ किसी व्याकरण के माध्यम से नहीं बनाई गईं हैं,ये तो बोलचाल की भाषाएँ होती हैं, जिनमें अधिकतर की अपनी लिपि नहीं होती है।
(ii) ये भाषाएँ प्रकृति, कृषि, ऋतुओं, जानवरों, औषधीय पौधों और जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती हैं।
(iii) ज्ञान का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से होता है। ये भाषा ही होती है जो पहचान बताती है उस समुदाय की जो ताल्लुक रखता है अपने पूर्वजों के अनुभवों से और अपनी संस्कृति को दर्शाता है।
(iv) ये भाषाएं याद दिला देती है उस इतिहास की, जिसके माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता मजबूत थी। आदिवासी अपनी परंपराओं पर खरे उतरते हैं।
संकट के मुख्य कारण
(i) शिक्षा प्रणाली में स्थान न होने का कारण है कि विद्यालयों में मुख्यधारा की भाषाओं (जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी) को प्राथमिकता दी जाती है। जिससे उनको अपनी भाषा को दर्शाने का मौका नहीं मिल पाता है।
(ii) जनजातीय भाषा को बोलने वालों की संख्या में कमी या युवा पीढ़ी में अपनी भाषा के प्रति झिझक या हीन भावना भी मुख्य कारण हो सकता है।
(iii) शहरीकरण और प्रवास भी एक कारण हो सकता है । गाँवों से शहरों की ओर पलायन करने पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग घटता है।
(iv) मीडिया और मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो आदिवासी भाषाओं में सामग्री की कमी भी कह सकते हैं।
आदिवासी संस्कृति पर नजर (विविधता और महत्व):
▪️कला: चित्रकला (जैसे गोंड, वारली), मूर्तिकला, हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। इनके सौंदर्य का वर्णन बहुत रोचक है।
▪️नृत्य और संगीत: इनकी धार्मिक, सामाजिक और कृषि पर्वों से गहरी जुड़ाव होता है। इनके गीत सुनकर लोगों को वसंत ऋतु न होते हुए भी उसका अहसास करवा देते हैं।
▪️पहनावा और आभूषण: स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते है।
▪️खानपान: पारंपरिक व्यंजन और औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं। पूरी तरह वनों/जंगलों पर निर्भर होते हैं।
▪️पारंपरिक ज्ञान: जैव विविधता, मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का अनुभवजन्य ज्ञान रखते हैं।
संकट के मुख्य कारण:
▪️बाहरी प्रभावों और पश्चिमी संस्कृति की नकल
▪️स्थानीय त्यौहारों और परंपराओं की उपेक्षा।
▪️बाजार आधारित व्यवस्था में पारंपरिक कारीगरी का मूल्य गिरना।
▪️धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों पर कानूनी और सामाजिक प्रतिबंध।
आइए जानते है संरक्षण के कुछ प्रयास जिनको कैसे अपनाया जा रहा है ?
सरकारी पहल:
(1) संविधान में मान्यता दी गई है। भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार देता है।
(2) पांचवीं और छठवीं अनुसूची के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई है।
(3) TRIFED और वन धन योजना के अनुसार आदिवासी उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य दिलाया जाता है।
(4) राज्य शैक्षिक बोर्ड और NCERT के माध्यम से कुछ राज्यों में आदिवासी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की गई है।
गैर-सरकारी और जन भागीदारी:
(1) कई NGOs और शैक्षणिक संस्थान आदिवासी भाषाओं के दस्तावेजीकरण और शिक्षण के प्रयास में लगे हैं।
(2) डिजिटल माध्यमों से स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयास (जैसे मोबाइल ऐप, यूट्यूब चैनल) किए जा रहे हैं।
(3) कुछ समुदायों ने अपनी भाषाओं के लिए लिपि तैयार की है, जैसे ओल चिकी (संथाली के लिए), जिससे आदिवासी भाषाएं अपने स्तर पर टिकी रहे।
संरक्षण की रणनीतियाँ कैसे अपनाए :
भाषा संरक्षण के उपाय:
• दस्तावेजीकरण: बोलचाल की भाषाओं को रिकॉर्ड करके उनके शब्दकोश, व्याकरण और लोक साहित्य का संकलन कर लेना चाहिए।
• शिक्षा में समावेशन: प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी भाषा में सहजता महसूस करें। यह सबसे सरल और बढ़िया विकल्प है।
• तकनीकी उपयोग: मोबाइल ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि में आदिवासी भाषाओं का उपयोग बढ़ाना चाहिए। जिससे लोग सुन सुन कर अपनी मातृभाषा में रुचि रखें और कहीं भी बोलने में हिचकिचाएं नहीं।
• आदिवासी भाषाओं में साहित्य और लोककथाओं को प्रकाशित करना चाहिए।
संस्कृति संरक्षण के उपाय:
• स्थानीय पर्वों और परंपराओं को मान्यता होनी चाहिए।
• आदिवासी कला और शिल्प को प्रोत्साहन व बाज़ार उपलब्ध कराना चाहिए
• युवाओं को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करना चाहिए। जिससे उनकी रुचि और प्रबल हो सके।
• स्थानीय समुदाय को ही संरक्षण में भागीदार बनाना चाहिए और उनको प्रेरित करने के प्रयास करते रहना चाहिए।
आदिवासी भाषाएँ और संस्कृति भारत की जीवंत धरोहर हैं। इनकी रक्षा करना मात्र संवैधानिक या सरकारी कर्तव्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि इनका संरक्षण नहीं हुआ, तो हम अपनी परंपरागत ज्ञान प्रणालियों, विविधता और सांस्कृतिक विरासत से वंचित हो जाएंगे।
संरक्षण का अर्थ केवल संग्रह करना नहीं, बल्कि इन्हें जीवित रखना है भाषा में बोलचाल, संस्कृति में जीवन।
आध्यात्मिकता के अनुसार मानव धर्म क्या है?
आध्यात्मिकता केवल किसी धर्म विशेष का पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता, मानवता, और सृष्टि से जुड़ाव की भावना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानव धर्म का अर्थ है:
• सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना
• प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना
• सत्य, अहिंसा, और सह-अस्तित्व के मूल्यों का पालन करना
• अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना
• भिन्नताओं में एकता को पहचानना और उसका सम्मान करना
• आदिवासी जीवन शैली, प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव को दर्शाती है जो कि आध्यात्मिकता की सबसे सजीव मिसाल है।
यह बातें लिखित रूप से आसान हैं लेकिन आचरण में उतारना कठिन किंतु संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी अद्भुत भक्ति विधि बताई है जिसके साथ ये सब कुछ आसानी से किया जा सकता है। अंत में यही कहेंगे कि मानव धर्म का सही पालन केवल आध्यात्मिकता के अनुसार ही कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें साधना चैनल प्रतिदिन शाम 7:30 बजे।