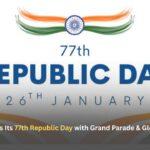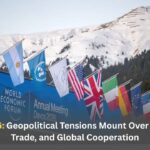यह तो बात बिल्कुल सत्य है कि भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है और इन गाँवों की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने का मुख्य कार्य करती हैं वहाँ की पारंपरिक शिल्पकालाएँ। इसका कारण यह है कि शिल्पकालाएँ न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति हैं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जीवनशैली, मूल्य और सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रमाण हैं। दुख की बात तो यह है कि वर्तमान में इन कलाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि आधुनिकता, तकनीकी विकास और बाजार की प्रतिस्पर्धा ने पारंपरिक ग्रामीण शिल्पों को हाशिए पर ला दिया है।
आज के युग में शिल्पकला में कोई रुचि नहीं लेता नजर आ रहा है। धीरे धीरे हमारे गाँव की परम्परा और संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में इन कलाओं का पुनर्जीवन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकता बन गया है।भारत देश की संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अधिक रोचक है। इसका मुख्य श्रेय सिर्फ हमारे देश के गाँव ों को जाता है ।
ग्रामीण शिल्पकला की परिभाषा और विविधता
‘शिल्पकला’ एक ऐसी पारंपरिक कला है जिसमें स्थानीय संसाधनों और कारीगरों की विशेषज्ञता के माध्यम से सजावटी या उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह कला अक्सर हाथों से की जाती है और इसमें स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों, धार्मिक विश्वासों और प्राकृतिक तत्वों का समावेश होता है। इसका उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग भी होता है। यह कला इंसानों के हाथ में भगवान की देन है, ऐसा माना जाता है। मुख्य बात तो यह है कि इस कला में किसी को अक्षर ज्ञान की भी जरूरत नहीं होती है। शिल्पकला के लिए सिर्फ व्यक्ति को रुचि होनी चाहिए, वह अपने आप दर्शाता है।
भारत की प्रमुख ग्रामीण शिल्पकालाएँ
भारत के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शिल्प परंपरा है:
मधुबनी चित्रकला (बिहार): मिथिला क्षेत्र की महिलाएं इसे मिट्टी की दीवारों और कपड़ों पर बनाती हैं, जिनमें प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक कथाओं का उपयोग होता है। दीवार पर चित्र के रूप में सुंदर कलाएं दर्शाई जाती हैं।
धोकरा कला (छत्तीसगढ़, बंगाल): धातु की यह मूर्तिकला आदिवासी समाज की लोककथाओं को जीवंत करती है। धातुओं द्वारा ये सुंदर कला मूर्ति के रूप में दर्शाई जाती है।
कांथा कढ़ाई (बंगाल): पुराने कपड़ों पर बारीक सिलाई से की जाने वाली यह कढ़ाई घरेलू जीवन के दृश्यों को चित्रित करती है। हाथों द्वारा रंगीन धागों की मदद से डिजाइन बनाई जाती हैं जो बहुत ही दुर्लभ और मनमोहक प्रतीत होती हैं।
ब्लू पॉटरी (जयपुर): फ़ारसी शैली से प्रभावित यह नीले रंग की मिट्टी की कारीगरी आज भी बहुत लोकप्रिय है।
पत्तचित्र (ओडिशा): ताड़पत्रों पर देवी-देवताओं की चित्रकारी की जाती है। पौराणिक कथाओं में से कुछ अंश लिए जाते हैं और उन्हें पत्तों पर चित्र के रूप में दर्शाए जाते हैं।
बिदरी वर्क (हैदराबाद): चाँदी की इनले वर्क के साथ काले धातु के बर्तन बनाए जाते है और उन पर फिर डिजाइन की जाती है।
इनके अलावा भारत में लाख की चूड़ियाँ, बुनाई, बेंत-बांस की वस्तुएँ, टेराकोटा मूर्तियाँ, और हाथ से बुने कपड़े भी शिल्पकला का हिस्सा हैं। जी हाँ, यदि आप बेंत बांस की कला देख लेंगे तो आपको यह अचंभा होगा कि ये इतनी दुर्लभ वस्तु बना कैसे दी और वो भी बिल्कुल हाथों के माध्यम से,जो बिल्कुल देखने में कठिन कार्य लगता है।
शिल्पकलाओं के लुप्त होने के मुख्य कारण
वर्तमान में आधुनिकता और मशीनीकरण को हम मुख्य कारण मानेंगे। विकास और तकनीकी प्रगति के साथ मशीनों से बनी वस्तुओं की माँग बढ़ गई है। ये वस्तुएं तेज़ी से बनती हैं, कम समय में अधिक वस्तुओं के निर्माण के कारण लोग मशीनीकरण। कोह महत्व देते है। मशीन के द्वारा बनाई गईं वस्तुएं बहुत सस्ती होती हैं और आसानी से उपलब्ध होती हैं। इससे शिल्पकारों के उत्पाद बाजार में पिछड़ जाते हैं और उनकी आय कम हो जाती है। आधुनिकता और मशीनीकरण द्वारा लोगों का रोजगार भी छीन लिया गया है।
युवा पीढ़ी की बेरुख़ी:
नई पीढ़ी पारंपरिक शिल्प को पिछड़ा हुआ काम समझती है। शिक्षा और शहरों की ओर पलायन के कारण युवा कारीगर इस पेशे को छोड़कर आधुनिक व्यवसायों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बच्चों की रुचि शिल्पकला में नहीं है इसका अहम कारण आधुनिकता और मशीनीकरण भी है । सरकारी सहयोग की कमी कई क्षेत्रों में कारीगरों को न तो पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है, न ही प्रशिक्षण, विपणन या ब्रांडिंग की सुविधाएं। इसके अलावा, बिचौलियों द्वारा शोषण भी एक बड़ी समस्या है।
शिल्पकलाओं का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व
सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक
हर शिल्पकला स्थानीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को प्रतिबिंबित करती है। जब हम एक मधुबनी चित्र देखते हैं, तो हमें बिहार की संस्कृति याद आती है। ये कलाएं हमारे समाज की अस्मिता का प्रतीक हैं।
रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण
शिल्पकला ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आत्मनिर्भर बनाती है। यह उन्हें सम्मानजनक आजीविका प्रदान करती है और ग्राम-स्तर पर आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देती है।
पर्यावरणीय संतुलन
ग्रामीण शिल्पों में प्रायः प्राकृतिक सामग्री जैसे कपास, बांस, मिट्टी, लकड़ी, और पुनर्नवीनीकरण वस्तुओं का प्रयोग होता है, जिससे ये पर्यावरण के लिए अनुकूल रहती हैं।
शिल्पकलाओं के पुनर्जीवन के प्रयास
भारत सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं:
हुनर हाट: शिल्पकारों को मंच देने की पहल।
अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
GI टैग (Geographical Indication): विशिष्ट शिल्प को कानूनी पहचान देने से उनकी पहचान और बाज़ार दोनों मजबूत होते हैं।
एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन: कई स्वयंसेवी संस्थाएं, जैसे Dastkar, SEWA, और Fabindia Foundation, कारीगरों को डिज़ाइन प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और बाज़ार में पहुँच प्रदान कर रही हैं।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स और ई-कॉमर्स: Amazon Karigar, Okhai, Etsy, और Indiacraft जैसे डिजिटल मंचों ने ग्रामीण शिल्पों को वैश्विक पहचान दिलाई है। अब कारीगर सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ पा रहे हैं, जिससे उनका मुनाफ़ा भी बढ़ा है।
हम और आप क्या कर सकते हैं?
स्थानीय शिल्पों को अपनाना
हमें अपने दैनिक जीवन में स्थानीय शिल्प से बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए – जैसे हस्तनिर्मित कपड़े, बर्तन, या सजावट की चीज़ें।
शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना
जब हम हस्तशिल्प मेलों, हाटों या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों से सीधे खरीदारी करते हैं, तो यह कारीगरों को आत्मबल और आय दोनों देता है।
बच्चों को शिल्पकला से जोड़ना
शिक्षा प्रणाली में शिल्पकला को स्थान देना और बच्चों को इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना इस कला को जिंदा रखने में मदद करेगा।
निष्कर्ष
भारत की ग्रामीण शिल्पकालाएँ केवल सुंदर वस्तुएं नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक ताने-बाने की आत्मा हैं। इनके लुप्त होने से केवल एक कला नहीं, बल्कि हमारी पहचान भी खतरे में पड़ती है। इसलिए इन कलाओं को बचाना, संरक्षित करना और पुनर्जीवित करना हमारी जिम्मेदारी है न केवल सरकार की, बल्कि हर नागरिक की। जब हम स्थानीय शिल्प को अपनाते हैं, तो हम न केवल एक उत्पाद खरीदते हैं, बल्कि एक परंपरा को जीवित रखते हैं।
इसके लिए हमें स्कूलों में बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और शिल्पकला से जुड़ी गतिविधियां भी करवाना चाहिए। शिल्पकला से जुड़ी गतिविधियां यदि बच्चे करेंगे तो उनके अंदर इसके प्रति रुचि जागृत होगी और हमें आशा होगी की हमारे देश की संस्कृति विलुप्त नहीं होगी। इसके लिए सरकार को भी अहम भूमिका निभानी चाहिए, जिससे लोगों में और ज्यादा हर्ष के साथ इन कलाओं को दर्शाने की मंशा जागृत होगी।