डिजिटल कैद में बीत रहा बचपन: भारत में बच्चों पर बढ़ता स्क्रीन एडिक्शन का संकट
2025 की ताज़ा रिपोर्टों से पता चला है कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रतिदिन औसतन 2.2 घंटे डिजिटल स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम खतरनाक माना जाता है।
यह न केवल नींद और मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है, बल्कि बच्चों की भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी गहरा असर डाल रहा है। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (National Family Health Survey) और एम्स (AIIMS) रायपुर जैसी संस्थाओं ने इस चलन को लेकर गहरी चिंता जताई है।
बढ़ती डिजिटल निर्भरता के पीछे का सच
भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच ने लोगों की जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहाँ डिजिटल संसाधन केवल वयस्कों के लिए माने जाते थे, अब बच्चे भी इनके आदी हो चुके हैं। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय के 33% छात्र स्क्रीन एडिक्शन के शिकार पाए गए हैं, जो पिछले आंकड़ों से कहीं अधिक है।
स्क्रीन एडिक्शन कुछ चौंकाने वाले आंकड़े:
1. भारत में 70 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूज़र्स और 60 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूज़र्स हैं।
2. महाराष्ट्र में 9 से 17 वर्ष के 22% बच्चे प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक स्क्रीन पर समय बिताते हैं।
3. 5 साल से कम उम्र के बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम 2.2 घंटे हो गया है।
4. 35% युवतियाँ सोशल मीडिया की वजह से मानसिक तनाव और आत्म-संदेह का सामना कर रही हैं।
5. 15% युवा लड़के गेमिंग की लत में फँसे हुए हैं।
6. 18–24 वर्ष के 27% युवा “समस्याजनक इंटरनेट उपयोग” (‘Problematic Internet Use’) (PIU) से पीड़ित हैं – ये वो लोग हैं जिनका इंटरनेट का उपयोग अस्वस्थ मानसिक स्थिति की ओर इशारा करता है।
बच्चों पर स्क्रीन एडिक्शन का प्रभाव
स्क्रीन की लत के कारण बच्चों में गंभीर मानसिक और शारीरिक लक्षण देखने को मिल रहे हैं:
- चिड़चिड़ापन और गुस्सा
- नींद की कमी (Insomnia)
- ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई
- सामाजिक अलगाव
- बोलचाल और बातचीत में गिरावट
- भावनात्मक अस्थिरता और अकेलापन
- स्क्रीन टाइम जितना अधिक होता है, बच्चों में वास्तविक दुनिया से संपर्क उतना ही कम होता जाता है। इससे ADHD, डिजिटल थकान, और यहां तक कि तनाव आधारित विकार तक पनपने लगते हैं।
मनोवैज्ञानिकों की सलाह क्या है?
देश के शीर्ष बाल मनोवैज्ञानिकों ने अभिभावकों और शिक्षकों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:
- स्क्रीन टाइम के लिए स्पष्ट सीमाएं तय करें।
- मोबाइल और टैबलेट को सोने से पहले और भोजन के समय बंद कर दें।
- बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों जैसे चित्रकला, कहानी लेखन, या पज़ल्स में व्यस्त रखें।
- हर सप्ताह बच्चों को आउटडोर खेलकूद के लिए प्रेरित करें।
- अगर बच्चा गुस्सैल या अत्यधिक मौन हो जाए तो मनोवैज्ञानिक परामर्श लें।
समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं
आजकल किशोरों और युवाओं में भी स्क्रीन एडिक्शन का खतरा तेज़ी से फैल रहा है। सोशल मीडिया पर रील्स देखने, गेमिंग, और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कार्य युवाओं में डोपामिन निर्भरता बढ़ा रहे हैं।
इस लत की वजह से न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि भावनात्मक संबंध और स्वस्थ संवाद भी कम होता जा रहा है।
क्या भारत के पास कोई स्क्रीन एडिक्शन नीति है?
वर्तमान में भारत सरकार के पास बच्चों और युवाओं की डिजिटल भलाई (Digital Wellbeing) से संबंधित कोई सशक्त राष्ट्रीय नीति नहीं है। हालाँकि, अदालतें और स्वास्थ्य संस्थान बार-बार इस ओर ध्यान दिला चुके हैं कि स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस नीति आवश्यक है।
बच्चों के लिए उपयोगी सुझाव: स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण कैसे रखें?
- घर में एक “नो मोबाइल ज़ोन” निर्धारित करें जैसे डाइनिंग एरिया या बेडरूम।
- सप्ताह में एक दिन “स्क्रीन-फ्री डे” रखें।
- बच्चों को तकनीक के लाभ और नुकसान के बारे में संवाद के माध्यम से जागरूक करें।
- अभिभावक स्वयं भी स्क्रीन उपयोग में नम्रता और अनुशासन दिखाएं, बच्चे अनुकरण करते हैं।
- परिवारिक गतिविधियाँ बढ़ाएं जैसे सामूहिक खेल, कहानियाँ सुनाना, पूजा आदि।
डिजिटल साधनों का सही उपयोग: तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का संदेश
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का यह स्पष्ट निर्देश है कि डिजिटल साधनों का उपयोग केवल सद्विचार और भक्ति मार्ग में होना चाहिए। वे बताते हैं कि परमात्मा ने ये तकनीकी सुविधाएं मनुष्य को दी हैं ताकि वह सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सके, अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके और मोक्ष की ओर अग्रसर हो।
उनके अनुयायी इस डिजिटल युग में भी स्क्रीन का प्रयोग केवल:
- आध्यात्मिक ई-बुक्स से ज्ञान लेने
- ऑनलाइन सत्संग सुनने
- सद्ग्रंथों का अध्ययन करने
और ईश्वर की भक्ति में समय लगाने के लिए करते हैं। इस तरह वे रील्स, गेमिंग, या नकारात्मक कंटेंट से बचते हैं और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं।
👉 अधिक जानकारी के लिए देखें:
बचपन में स्क्रीन की लत से जुड़े सवाल
1. स्क्रीन एडिक्शन क्या है?
स्क्रीन एडिक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा मोबाइल, टैबलेट, या अन्य डिजिटल स्क्रीन के बिना बेचैन हो जाता है और उनका अत्यधिक उपयोग उसकी दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को प्रभावित करने लगता है।
2. बच्चों के लिए सुरक्षित स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए?
5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटा और 6–18 साल के बच्चों के लिए 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए (WHO व अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं के अनुसार)।
3. स्क्रीन की लत बच्चों पर किस तरह असर डालती है?
यह नींद की गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, सामाजिक दूरी, और आंखों की थकान जैसी समस्याओं को जन्म देती है। लंबे समय में यह मानसिक विकारों का कारण भी बन सकती है।
4. माता-पिता बच्चों की स्क्रीन लत को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?
समय सीमा तय करें, स्क्रीन-मुक्त समय (जैसे डिनर टाइम) लागू करें, डिजिटल डिटॉक्स डे रखें, और बच्चों को आउटडोर व रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं।
5. क्या सिर्फ गेम्स और सोशल मीडिया ही स्क्रीन एडिक्शन के लिए ज़िम्मेदार हैं?
नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई, यूट्यूब वीडियोज़, और रील्स जैसी सामग्री भी अगर संतुलित रूप से न देखी जाए, तो लत बन सकती है।
6. स्क्रीन एडिक्शन और समस्याजनक इंटरनेट उपयोग (Problematic Internet Use) में क्या फर्क है?
स्क्रीन एडिक्शन विशेष रूप से मोबाइल/स्क्रीन पर समय बिताने से जुड़ा होता है, जबकि समस्याजनक इंटरनेट उपयोग एक व्यापक समस्या है जिसमें व्यक्ति ऑनलाइन कंटेंट, गेमिंग, सोशल मीडिया या किसी एक डिजिटल गतिविधि पर असामान्य रूप से निर्भर हो जाता है।
7. स्क्रीन टाइम के दौरान किस तरह की गतिविधियाँ कम हानिकारक मानी जाती हैं?
शैक्षणिक सामग्री देखना, ई-बुक्स पढ़ना, और रचनात्मक टूल्स (जैसे आर्ट ऐप्स) का सीमित समय तक उपयोग अपेक्षाकृत कम हानिकारक माने जाते हैं।
8. क्या स्क्रीन की लत का कोई इलाज संभव है?
जी हां, समय पर पहचान कर उचित काउंसलिंग, व्यवहार सुधार तकनीकों, डिजिटल डिटॉक्स, और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका से इससे छुटकारा पाया जा सकता है।

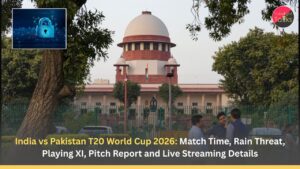


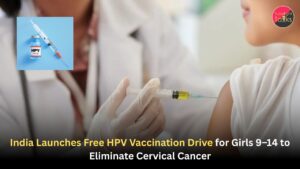
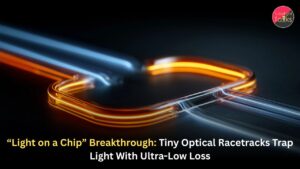





Discussion (0)